भारत में जल्द ही जनगणना होने वाली है लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला लिया है. मतलब साफ है कि आजादी के 78 साल बाद पहली बार देश में जातिगत जनगणना होगी. यहां आपको बता दें कि हिन्दुस्तान में अभी अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की गणना का प्रावधान है. लेकिन पिछड़ी और अन्य जातियों की गिनती अभी तक जनगणना में नहीं होती है.
लेकिन इस बार होने वाली जनगणना में ओबीसी समाज से जुड़ी जातियों की भी गिनती होगी और केंद्र की मोदी सरकार ने इसका रास्ता साफ कर दिया है. 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई CCPA की बैठक से जातिगत जनगणना को हरी झंडी मिल गई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जातिगत जनगणना, मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी.
खास बात यह है कि सरकार के इस कदम से विपक्ष भी उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है. विपक्षी नेता इसे अपनी जीत की तरह देख रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे.
विपक्षी नेता, जातिगत जनगणना के इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे और अपनी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने की बात करते थे. सरकार ने जातिगत आधारित जनगणना का फैसला लेकर विपक्ष के मुंह से यह मुद्दा छीन लिया है.
आखिर जातिगत जनगणना क्या है? आजाद भारत में क्यों पहली बार इसकी जरूरत पड़ी? सरकार कैसे जनगणना कराती है? 2021 में क्यों जनगणना नहीं हुई? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब हम इस लेख में आपको देंगे.
क्या है जातिगत जनगणना का मतलब?
जनगणना का सामान्य अर्थ होता है- जन (लोगों) की गिनती. वहीं अगर इसके आगे जातिगत लिखा है तो इसका मतलब है कि लोगों की जाति पूछकर उनके गिनती करना. इसका उद्देश्य है कि देश में किस जाति के कितने लोग निवास करते है. इसका पूरा ब्यौरा इकट्ठा करना. SC/ST समाज के साथ-साथ अब OBC समाज की जातियों की गिनती होगी. जिससे पता चलेगा कि देश में किस जाति के कितने लोग निवास करते हैं और समाज में उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति क्या है.
क्यों जातिगत जनगणना की जरूरत हुई महसूस?
साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था और पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया. उस वक्त सरकार ने 1931 की जनगणना को आधार मानकर आरक्षण की सीमा तय की. बता दें 1931 में देश में पिछड़ी जातियों की, संख्या कुल आबादी का 52 प्रतिशत ही थीं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछड़ों की आबादी का यह डेटा है 90 वर्ष से भी पुराना है. क्योंकि इसके बाद जातिगत जनगणना हुई ही नहीं तो मौजूदा समय में एग्जेक्ट डेटा का अनुमान लगाना कठिन है. उनका कहना है कि SC/ST को उनकी आबादी के आधार पर ही आरक्षण मिलता है. लेकिन ओबीसी समाज के आरक्षण का आधार 90 साल पुरानी जनगणना है. जो वर्तमान समय में प्रासंगिक ही नहीं है. इसलिए जातिगत जनगणना से इसका ठोस आधार होगा और उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण में बदलाव किया जा सकेगा.
भारत में जनगणना का इतिहास
भारत में सबसे पहली बार जनगणना साल 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी. हालांकि, यह एक प्रायोगिक जनगणना थी और इसे पूर्ण जनगणना नहीं माना जाता था.
वहीं पहली पूर्ण जनगणना साल 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कराई गई थी. इसी जनगणना में पहली बार जातिगत आकंडे जारी हुए थे. जिसके बाद से हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है. 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकडे जारी किए गए. वहीं 1941 में भी जनगणना के आकंड़े जुटाए गए लेकिन इन्हें पब्लिक नहीं किया गया.
आजादी के बाद जनगणना
आजादी के बाद साल 1951 में पहली बार जनगणना हुई लेकिन जाति आधारित नहीं. नेहरू कैबिनेट की पहली बैठक (जिसमें सरदार पटेल, आंबेडकर और मौलाना आजाद जैसे नेता थे) में जातिगत जनगणना नहीं कराने की बात तय हुई. उनका मानना था कि ये कदम समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है.
1951 से लेकर 2011 तक सभी 7 जनगणनाओं में सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की ही गिनती कराई. क्योंकि उन्हें आरक्षण देने के लिए संवैधानिक बाध्यता थी. ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाली जातियों का कोई सर्वे नहीं हुआ.
जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष में तर्क
पक्ष- जो लोग जातिगत जनगणना चाहते हैं उनका कहना है कि इससे समाज में पिछड़े-अतिपिछडे लोगों की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का पता चल सकेगा. उसी हिसाब से उनके उत्थान के लिए सरकार को उचित नीति और योजनाओं का कार्यन्यवयन करेगी. यह समाज में एक रस लाने और भारत और आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा.
विपक्ष- जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे समाज में जातीय विभाजन बढ़ेगा. लोगों के बीच कटुता बढ़ेगी. जातिगत जनगणना सामाजिक ताने-बाने को बिखरने का काम करेगी.
पिछली बार कब हुई थी जनगणना?
भारत में जनगणना हर 10 साल के अंतराल पर होती है. भारत में आखिरी बार जनगणना साल 2011 में हुई थी. इसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह जनगणना नहीं हो सकी. इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है. सूत्रों के मुताबिक, इस साल (2025) में जनगणना शुरू हो सकती है और इसे पूरा होने में 1 साल का समय लग सकता है यानि कि 2026 के अंत तक या 2027 के शुरूआत में जनगणना के आकंड़े सार्वजनिक हो जाएंगे.
2011 की जनगणना में क्या-क्या पूछे सवाल?
2011 में जनगणना आयुक्त सी. चंद्रमौली के नेतृत्व में जनगणना संपन्न हुई थी. उस समय जनगणना के फॉर्म में 29 कॉलम थे. जिनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार जैसी जानकारी भरनी होती थी. इसके अलावा में SC/ST वर्ग का भी एक कॉलम था. इसमें इससे संबंधित सभी जातियों की डिटेल भरनी थी.
फॉर्म के 29 कॉलम
1. नाम
2. परिवार के मुख्या से रिश्ता
3. लिंग
4. उम्र
5. वैवाहिक स्थिति
6. आयु
7. जन्मस्थान
8. धर्म
9. SC/ST- सभी जातियों की डिटेल
10. डिसीबिलिटी
11. मातृभाषा
12. अन्य भाषा का ज्ञान
13. शैक्षिक योग्यता
14. हायर एजुकेशन
15. रोजगार की स्थिति
16. बच्चे की स्कूल में उपस्थिति
17. ऑर्थिक सोस्र
18. वर्तमान काम
19. नौकरी या सेल्फ इम्पलॉय
20. काम की श्रेणी
21. अगर काम नहीं करते
22. काम की तलाश
23. काम करने के लिए कितनी दूर और कैसे जाते हैं
24. माइग्रेशन की स्थिति
25. देश छोड़ा और क्यों
26. कितने समय के लिए छोड़ा
27. बच्चों की स्थिति
28. कुल कितने बच्चे पैदा हुए थे.
29. पिछले एक साल में जो बच्चा हुआ वो बचा या नहीं
भारत के किस राज्य में जातिगत जनगणना हुई?
भारत में अबतक दो राज्यों में ही जातीय सर्वे हुआ है. पहला राज्य है बिहार और दूसरा कर्नाटक. इसके अलावा तेलंगाना ने भी जातिगत सर्वेक्षण कराया है. इसमें पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा आबादी निकल कर सामने आई है.
संविधान में जनगणना का प्रावधान
भारत के संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत जनगणना संघ सूचि का विषय है. यह संविधान की सातवीं अनुसूची के 69 नंबर में सूचीबद्ध है. यानि जनगणना कराने और उससे संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है. जबकि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है. इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से समवर्ती सूचि में जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि इस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं.
दरअसल, राज्य सरकारें जनगणना नहीं करा सकती हैं. यह काम केवल केंद्र सरकार करती है. इसलिए राज्य सरकार इसे सर्वे का नाम देती हैं.
जातिगत जनगणना के लिए क्या कानून में करना होगा संशोधन?
बता दें जनगणना एक्ट 1948 में केवल एससी-एसटी वर्ग की गणना का ही प्रावधान है. सरकार को ओबीसी की गणना के लिए इस एक्ट में संसोधन करना होगा. इससे ओबीसी की 2,650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे. 2011 की जनगणना के अनुसार, 1,270 एससी, 748 एसटी जातियां हैं.
कैसे होती जनगणना?
जनगणना कराने का दायित्व भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आय़ुक्त कार्यालय के पास होता है. यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है. ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, जनगणना दो चरणों में कराई जाती है. पहला है हाउसिंग- जिसमें घर में बिजली, पेयजल, शौचालय और संपत्ति पर कब्जे से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. वहीं दूसरी फॉर्म नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का होता है. इसमें इसमें घर के सदस्यों से जुड़े सवाल दर्ज होते हैं.
जनगणना के लिए सरकारी कर्मचारियों (टीचर, आंगनवाड़ी वर्कस आदि) की नियुक्ति होती है, इन्हें एन्यूमेरेटर कहते हैं. ये ग्राउंड जीरो पर जाकर कई तरह की जानकारियों को जुटाते हैं. सरकार इन्हें खास तरह का पहचान पत्र देती है. किसी भी तरह की संशय की स्थिति में आम इंसान इनसे आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने को कह सकता है.
आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या है फैसला
देश के सर्वोच्च न्यायलय ने अपने एक फैसले में सरकारी नौकियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती. वहीं अगर जातिगत जनगणना में ओबीसी की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा निकली तो क्या इस सीमा को तोड़ दिया जाएगा? यह बड़ा सवाल है.
2011 जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण आकंड़े
– 2011 की जनगणना 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी.
– 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही.
– साक्षरता दर- 74.04% जो 2001 के मुकाबले 9.21 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है.
– पुरुष (82.14%) और महिलाएं (65.46%) साक्षरता दर
किस धर्म के कितने लोग
– 20.24 करोड़- हिंदू
– 3.12 करोड़- मुसलमान
– 6.3 करोड़- ईसाई
– 4.1 करोड़- सिख
– 1.9 करोड़- जैन
सबसे अधिक आबादी वाले राज्य (2011 जनगणना)- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश
2011 जनगणना के सामान्य प्रश्न और उत्तर
- सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य
बिहार - सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य
अरुणाचल प्रदेश - सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश
लक्षद्वीप - सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य
उतार प्रदेश - सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य
सिक्किम - सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य
केरल - सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य
हरयाणा - सर्वोच्च साक्षरता दर वाला राज्य
केरल - सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य
बिहार
ये भी पढ़ें- जातिगत जनगणना कराएगी मोदी सरकार, CCPA की बैठक में केंद्र का बड़ा फैसला


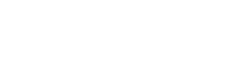
















कमेंट